भारत सावित्री Bharat Savitri
₹350.00
| AUTHOR: | Vasudevsharan Aggarwal |
| SUBJECT: | भारत सवित्री | Bharat Savitri – Bhagwadgita |
| CATEGORY: | History |
| LANGUAGE: | Hindi |
| EDITION: | 2021 |
| PAGES: | 800 |
| BINDING: | Hard Cover |
| WEIGHT: | 970 GRMS |
प्रकाशकीय
हमारे प्राचीन साहित्य में जिन महान् ग्रन्थों को असाधारण लोकप्रियता प्राप्त हुई हैं, उनमें महाभारत का अपना स्थान है। भारत का शायद ही कोई ऐसा शिक्षित और अशिक्षित परिवार हो, जिसमें महाभारत का नाम न पहुंचा हो और जो उसकी महिमा को न जानता हो। रामायण की भांति इस अमर ग्रन्थ को भी बड़ा धार्मिक महत्त्व प्राप्त है और इसकी कथा सर्वत्र बड़े चाव और आदर भाव से पढ़ी और सुनी जाती है।
निस्संदेह महाभारत ज्ञान का भण्डार और रत्नों की खान है। सागर की भांति इसमें जो जितनी गहरी डुबकी लगाता है, उसे उतने ही मूल्यवान रत्न प्राप्त होते हैं।
हमें हर्ष है कि प्रस्तुत पुस्तक भारत सवित्री में भारतीय साहित्य के अध्येता तथा चिन्तक श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस महान् ग्रन्थ का एक नवीन एवं सारगर्भित अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन वस्तुतः एक नई दृष्टि प्रदान करता है। स्थानाभाव के कारण यद्यपि बहुत से विवरण उन्हें संक्षिप्त कर देने पड़े हैं, तथापि महत्त्व के प्रायः सभी विवरण इसमें आ गये हैं।
जैसा कि लेखक ने अपनी भूमिका में संकेत किया है, यह पुस्तक भारत सवित्री तीन खण्डों में प्रस्तुत की गई है। ‘विराट पर्व’ तक की सामग्री पहले खण्ड में आ गई है। युद्ध के अन्त तक का अंश दूसरे खण्ड में, शेष तीसरे खण्ड में। इस प्रकार इन तीनों खण्डों में सम्पूर्ण महाभारत का सार पाठकों को मिल जाता है।
हिन्दी में अपने ढंग का यह पहला प्रकाशन है। इसकी सामग्री न केवल रोचक है, अपितु वह महाभारत के सूक्ष्म अध्ययन के लिए पाठकों को एक नई प्रेरणा देती है।
हमें विश्वास है कि इस ग्रन्थ का अध्ययन पाठकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
भूमिका
‘भारत सावित्री’ के रूप में महाभारत का एक नया अध्ययन यहां प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन के अट्ठाइस लेख ‘हिन्दुस्तान’ साप्ताहिक पत्र में धारावाहिक रूप से १६५३-५४ में प्रकाशित हुए थे, शेष अंश बाद में लिखा गया है। पुस्तक तीन खण्डों में है। इस प्रथम खण्ड में ‘विराट पर्व’ तक की कथा आ गई है। दूसरे खण्ड में ‘उद्योग पर्व’ से ‘स्त्री पर्व’ अर्थात् युद्ध के अन्त तक की कथा है और तीसरे खण्ड में ‘शान्ति पर्व’ से लेकर महाभारत के अन्त तक का अंश दिया गया है।
‘भारत सावित्री’ नाम महाभारत के अन्त में आया है। जैसे वेदों का सार गायत्री मन्त्र या सावित्री है, वैसे ही सम्पूर्ण महाभारत का सार धर्म शब्द में है। भारत-युद्ध की कथा तो निमित्त मात्र है, इसके आधार पर महाभारत के मनीषी लेखक ने युद्ध कथा को धर्म-संहिता के रूप में परिवर्तित कर दिया था। धर्म की नित्य महिमा को बताने के लिए ग्रन्थ के अन्त में यह श्लोक है :
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद् धर्मं त्यजेज्जीवितास्यापि हेतोः ।
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये नित्यो जी धातुरस्य त्वनित्य ।।
(स्वर्गा० ५। ६३, उद्योग० ४०।११-१२ )
अर्थात् काम से, भय से, लोभ से अथवा प्राणों के लिए भी धर्म को छोड़ना उचित नहीं । धर्म नित्य है, सुख और दुःख क्षणिक हैं। जीव नित्य है और शरीर (धातु) अनित्य है। इस श्लोक की संज्ञा भारत सावित्री है (स्वर्गा० ५। ६४) । यही महाभारत का निचोड़ या उसका गायत्री मन्त्र है। विश्व की प्रेरक शक्ति का नाम सविता है। महाभारत ग्रन्थ का जो धर्मप्रधान उद्देश्य है, वही उसका सविता देवता है। उसकी प्रेरणात्मक भावना को इस अध्ययन में यथासम्भव सुरक्षित रखा गया है। यही इस नाम का हेतु है।
वेदों में सृष्टि के अखण्ड विश्वव्यापी नियमों को ऋत कहा गया था। ऋत के अनुसार जीवन का व्यवहार मानव के लिए श्रेष्ठ मार्ग था। ऋत के विपरीत जो कर्म और विचार थे, उन्हें वरुण का पाश या बन्धन समझा जाता था। वैदिक परिभाषाओं का आनेवाले युग में विकास हुआ। उस समय जो शब्द सबसे ऊपर तैर आया, वह धर्म था। धर्म शब्द भारतीय संस्कृति का सार्थक और समर्थ शब्द बन गया।
महाभारतकार ने धर्म की एक नई व्याख्या रखी है, अर्थात् प्रजा और समाज को धारण करनेवाले, नियमों का नाम धर्म है। जिस तत्त्व में धारण करने की शक्ति है, उसे ही धर्म कहते हैं :
धारणाद्धर्म इत्याहुधर्मो इत्याहुधर्मो धारयते प्रजाः ।
यत्स्याद्धारण संयुक्तं स धर्म इत्युदाहृतः ।।
जितना जीवन का विस्तार है, उतना ही व्यापक धर्म का क्षेत्र है। धर्म की इस व्याख्या के अनुसार धर्म जीवन का सक्रिय तत्त्व है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की निजी स्थिति और लोक की स्थिति सम्भव बन रही हैं। धर्म, अर्थ, काम की संज्ञा त्रिवर्ग है। इस त्रिवर्ग में भी धर्म ही मुख्य है एवं राज्य का मूल भी धर्म ही है :
त्रिवर्गोऽयम् धर्ममूलं नरेन्द्र राज्यं चेदं धर्ममूलं वदन्ति ।
धर्म अथवा मोक्ष के विषय में भी जो कुछ मूल्यवान अंश महाभारत में है, उसपर प्रस्तुत अध्ययन में विशेष ध्यान दिया गया है।
ब्रह्मवाद और प्रज्ञावाद के सम्मिलन से जीवन के जिस कर्मपरायण एवं उत्थानशील मार्ग की उद्भावना प्राचीन भारत में की गई थी, उसका बहुत ही रोचक और सर्वोपयोगी वर्णन महाभारत में पाया जाता है। गृहस्थ जीवन का निराकरण करने वाले श्रमणवाद और कर्म का तिरस्कार करनेवाले नियतिवाद या भाग्यवाद का सक्षम उत्तर इस नए धर्मप्रधान दर्शन का उद्देश्य था। भुक्ति-मुक्ति अर्थात् त्रिवर्ग और मोक्ष इन दोनों के समन्वय का आग्रह उस धर्म की विशेषता है, जिसका प्रतिपादन महाभारत में हुआ है। महाभारत के तरंगित कथा प्रवाह में जहां-जहां ये स्थल आये हैं और उनकी संख्या पर्याप्त है उनकी रोचनात्मक व्याख्या इस अध्ययन में इष्ट रही है।
साथ ही महाभारत में जो सांस्कृतिक सामग्री है, उसकी व्याख्या का पुट भी यहां मिलेगा, यद्यपि इस विषय में सब सामग्री को विस्तार के साथ लेना स्थानाभाव से सम्भव नहीं था।
पूना से महाभारत का जो संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ है, उस पाठ को आधार मानकर यह विवेचन किया गया है। जहां सम्भव था, वहां यह सूचित करने का भी प्रयत्न किया गया है कि महाभारत के पाठ-विकास की परम्परा में कौन-सा अंश मौलिक और कौन-सा मूल के उपबृंहण का परिणाम था। इसमें दो विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। एक तो, जहां किसी प्रकरण या आख्यान के अन्त में फलश्रुति का उल्लेख हुआ है, वह अंश उपबृंहण का फल माना गया है। दूसरे, जहां किसी कथांश को एक बार संक्षेप में कहकर पुनः उसी को विस्तार से सुनने या कहने की प्रार्थना की गई है
वह अंश भी प्रायः उपबृंहण या पाठ-विस्तार का ही परिणाम था। प्रायः जनमेजय पूछते हैं, “भगवन्, मैं इसे अब विस्तार से सुनना चाहता हूं।” (विस्तरेणैतदिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज, सभा० ४६ । ३ । और उत्तर में वैशम्पायन कहते हैं, “हे भारत, अब इसी कथा को में विस्तार से सुनाता हूं।” (शृणु मे विस्तरेणेमां कथ भरतसत्तम। भूय एव महाराज यदि ते श्रवणे मतिः ।।
विस्तार से फिर सुनाने की बात जहां है, वहां स्पष्ट ही वह पुनरुक्ति है, जैसाकि इसी के आगे सभा पर्व के ४६, ४७ और ४८ अध्यायों की भौगोलिक और सांस्कृतिक सामग्री को देखने से प्रकट होता है। इसी प्रकार सभा पर्व के २३ वें अध्याय में चारों दिशाओं की विजय संक्षेप में सुनने के बाद जनमेजय ने पूछा, हे ब्रह्मन् ! अब दिशाओं की विजय विस्तार से कहिये, क्योंकि पूर्वजों का महान् चरित्र सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती।” (दिशामभिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणानु कीर्तय। न हि तृप्यामि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं महत् ।। सभा० २३ । ११) । फलस्वरूप इसके बाद के सात अध्यायों में दिग्विजय का विस्तृत वर्णन है।
महाभारत की पाठ-परम्परा में इसके कई संस्करण सम्भावित ज्ञात होते हैं। उनमें से एक शुंगकाल में और दूसरा गुप्तकाल में सम्पन्न हुआ जान पड़ता है। इनमें भी पिछले संस्करण में पंचरात्र भागवतों ने बहुत सी नई सामग्री अपने अभिनव दृष्टिकोण के अनुसार यथास्थान सन्निविष्ट कर दी थी। उसकी ओर भी प्रस्तुत अध्ययन में ध्यान दिलाया गया है। जीवन और धर्म के विषय में भागवतों का जो समन्वयात्मक शालीन दृष्टिकोण था, उससे महाभारत के कथा-प्रसंगों में नई शक्ति और सरसता भर गई है। भागवतों का विशेष आग्रह धर्म के उस स्वरूप पर था, जिससे समाज की प्रतिष्ठा गृहस्थाश्रम की महिमा प्रख्यात होती है। प्रायः भागवत दर्शन प्राचीन प्रज्ञावाद और ब्रह्मवाद का ही एक नूतन संस्करण था ।
महाभारत के कथा-प्रवाह का सबसे रोचक अंश उसके देवतुल्य पात्रों का चरित्र-चित्रण है। वे पात्र महान और अभिभावी होते हुए भी मानवीय है। वे मानव के धरातल पर कहते सुनते करते और सोचते हैं, यद्यपि सत्य की शक्ति और जीवन की अप्रतिहत अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनके कर्म और विचार अतिमानवी-से लगते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनके चरित्र की जो उदात्त भावनाएं हैं, या जो दुर्बलताएं हैं, उनको बिल्कुल खरे रूप में महाभारत के लेखक ने कहा है।
इनमें धृतराष्ट्र का चरित्र या द्रौपदी का चरित्र कितना मानवीय है, यह पाठकों को मूल के शब्दों से ही ज्ञात होगा। ऐसे अंशों को यथासम्भव अविकल रूप में उतार लेने का प्रयत्न किया गया है। भाषान्तर में भी उनके गूंजते हुए स्वरों को सुना जा सकता है। धृतराष्ट्र को महाभारत में दिष्टवादी या भाग्यवादी दर्शन का मानने वाला कहा है। पुरुषार्थ और कर्म में उनकी आस्था न थी। जो है, वह निर्विघ्न वैसा ही बना रहे, यहीं तक उनके विचार की दौड़ थी।
फिर दुर्योधन का मोह उनके मन में ऐसा भरा था कि नए संकल्प पर पानी फेर देता था। पाण्डवों को वारणावत भेजने का कुचक्र, जब दुर्योधन ने सामने रखा तो धृतराष्ट्र ने पहले तो कुछ पैंतरा बदला, पर फिर स्पष्ट स्वीकार किया, “बात तो कुछ ऐसी ही मेरे मन में है, पर खुलकर कह नहीं सकता” (पृ० ११२) । ऐसे ही अर्जुन और सुभद्रा के विवाह का समाचार सुनकर पहले उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की, पर दुर्योधन और कर्ण के चांपने पर कहा, “जैसा तुम कहते हो, सोचता तो मैं भी वही हूं, पर विदुर के सामने खुलकर अपनी बात कह नहीं सकता” (पृ० १२३)। पाण्डवों के साथ द्यूत खेलने का प्रस्ताव चलने पर धृतराष्ट्र के सही विचारों ने एक बार उछाला लिया, पर भाग्यवाद की गोली ने उन्हें सुला दिया और उन्होंने यही कहा, “ब्रह्मा ने जो रच दिया है, सारा जगत् वैसी ही चेष्टा में लगा हुआ है” (पृ० १७२) । जब युधिष्ठिर द्यूत में हारने लगे, तो धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर बार-बार पूछते हैं, “क्या सचमुच जीत लिया ?” और वह अपनी मुद्रा छिपा न सके ( पृ० १७६) ।
यों तो महाभारत के लेखक ने युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि के चरित्रों को भी बहुत ही तराशे हुए खरे शब्दों में ढाला है, पर धृतराष्ट्र के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जैसे चुटीले शब्द चुने गए हैं, वैसे औरों के लिए नहीं। पाण्डवों को दूसरी बार द्यूत-क्रिया में लगाने का प्रस्ताव जब दुर्योधन ने किया, तब भी उसको बरजने के स्थान में धृतराष्ट्र से यही कहते बना, “हां हां, अभी पाण्डव रास्ते में होंगे, उन्हें जल्दी लौटा लाओ” (पृष्ठ १८६) ।
विदुर का हितवचन भी धृतराष्ट्र के मन में उल्टे विष उत्पन्न करता था, यहांतक कि एक बार तो विदुर को उन्होंने अपने यहां से निकाल ही दिया था, “मैं पाण्डवों के लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ दूं ? मैं तो तुम्हारा इतना आदर करता हूं, पर तुम मुझसे सदा टेढ़ी बातें ही करते हो। हे विदुर ! तुम्हारा जहां मन हो, चले जाओ” (पृ० १६२) । पर बूढ़े धृतराष्ट्र में भी सचाई की कोर थी, जिससे वह भी हमारी सहानुभूति के पात्र हैं।
विदुर को भली-बुरी सुनाने के बाद वह स्वयं होश होकर गिर जाते है और कहते हैं “हाय मेरा भाई विदुर कहां गया ? उसे जल्दी लाओ।” चरित्र-चित्रण में लेखक ने बहुत ही सचाई से रंग भरा है। अवसर पड़ने पर शकुनि-जैसे कपटी के मुंह से भी कहलाया गया है, “पाण्डव सत्यवादी हैं। वे शर्तों का पालन करेंगे और धृतराष्ट्र के बुलाने पर भी तेरह वर्ष का वनवास पूरा किये बिना वे न लौटेंगे।”
कथा-प्रवाह में द्रौपदी का चरित्र बरबस अपनी ओर ध्यान खींचता है। उसकी वेदना शब्दों के बन्धन में नहीं आती। जैसे सहसा किसी को काठ मार गया हो, वैसे उसके वचन कृष्ण के सामने प्रकट होते हैं, “पाण्डवों की पत्नी, कृष्ण की सखी, पृष्टद्युम्न की बहन सभा में लाई गई को कृष्ण, यह क्या हुआ ? एक वस्त्र पहने हुई, स्त्री-धर्म से युक्त, मुझ दुखिया को राजसभा में लाये हुए देखकर धृतराष्ट्र के पापी पुत्र निष्ठुरता से हंसे कहो कृष्ण यह क्या हुआ ?
क्या यह सत्य है कि मैं भीष्म और धृतराष्ट्र की पुत्रवधू हूं ?” (पृ० २००)। वह वेदना भरे शब्दों में कहती है, मैं धर्म को भला-बुरा नहीं कहती, ईश्वर और ब्रह्मा का निरादर तो कैसे कर सकती हूं ? इतना ही समझो कि मैं दुखिया हूं। कुछ प्रलाप करती हूं” (पृ० २०६) ।
महाभारत की एक अन्य विशेषता की ओर भी ध्यान दिलाना आवश्यक है। उसमें कितनी ही प्राचीन भारतीय दिट्ठियों या दर्शनों का उल्लेख और उनके सिद्धान्तों का भी विवेचन आ गया है। भारतीय दर्शनों के इतिहास में पांच बड़े मोड़ पहचाने जा सकते हैं। पहला ऋग्वेद-कालीन दर्शन था, जिसमें सदसद्वाद, रजोवाद, अम्भोवाद, अहोरात्रवाद अमृतमृत्युवाद, व्योमवाद आदि दार्शनिक दृष्टिकोण थे, जिनका उल्लेख ‘नासदीय सूक्त’ में आया है।
दूसरा युग उन दिट्ठियों का था, जो उपनिषद् युग के अन्त में और बुद्ध से कुछ पूर्व अस्तित्व में आ गई थीं। इनका उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद् में आया है, जैसे कालवाद, नियतिवाद, स्वभाववाद, यदृच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद आदि। इन मतों का विवेचन ‘दीर्घनिकाय’ के ‘ब्रह्मजालसुत्त’ में आया है एवं जैनों के अर्द्धमागधी आगम के ‘सूत्रकृतांग’ एवं ‘उत्तराध्ययन’ में भी है।
दार्शनिक विकास का तीसरा मोड़ मीमांसा, सांख्य, वेदान्त आदि षड्दर्शनों के रूप में देखा जाता है विकास की चौथी सीढ़ी पंचरात्र, भागवत, पाशुपत, शैव आदि दर्शनों के रूप में अभिव्यक्त हुई। इसके बाद पांचवां मोड़ वह था, जिसमें अभिनव शांकर वेदान्त, भक्ति आदि दर्शनों के पारस्परिक प्रभाव, सम्मिलन और ऊहापोह आदि का विस्तार हुआ।
इनमें से दार्शनिक विकास की जो दूसरी कोटि है, वही मूल महाभारत की पृष्ठभूमि थी, यद्यपि षड्दर्शन नामक तीसरी कोटि और पाशुपत पंचरात्र आदि चौथी कोटि का भी कालान्तर में महाभारत में सन्निवेश कर लिया गया। मंखलि गोसाल के नियतिवाद या भाग्यवाद और चार्वाक बृहस्पति के लोकायतवाद आदि दार्शनिक मतों का जैसा वर्णन महाभारत में आया है, पैसा बौद्ध और जैन साहित्य में भी नहीं मिलता।
यह सामग्री विशेष रूप से शान्ति पर्व की व्याख्या में हमारे सामने आयगी पर अन्य पर्वो में भी उसकी झांकी आती है, जैसे आरण्यक पर्व में द्रौपदी ने बृहस्पति के कहे हुए जिस नीति शास्त्र को दुहराया है, वह लोकायत दर्शन ही था, जो मूल में कर्मवादी था। प्रत्यक्ष जीवन को सुधारने के विषय में उनका आग्रह बहुत बढ़ा-चढ़ा था। जहां भाग्यवादी निर्वेद को मानते थे और कर्म के प्रति उदासीन थे, वहां महाभारत के इस प्रकरण से (आरण्यक पर्व, अ० ३३) ज्ञात होता है कि बृहस्पति के लोकायत दर्शन में अनिर्वेद, उत्थान, पुरुषार्थ और कर्म का बहुत महत्व था।
लोकायतिक मत के अनुयायी यदृच्छावाद, दैववाद और स्वभाववाद के दार्शनिक मतों में विश्वास न रखते थे ( पृ० २११-२१२) । इसी प्रकार आगे चलकर उद्योग पर्व में जो विदुर नीति है, वह प्रज्ञावाद नामक प्राचीन दर्शन का ही मूल्यवान संग्रह है, जो किसी प्रकार तैरता हुआ आकर महाभारत में बचा रह गया है। अगले भाग में यथास्थान इसकी व्याख्या मिलेगी। महाभारत की दार्शनिक सामग्री में जो पूर्वापर की जमी हुई तहें हैं, उनके आर-पार देखने की आंख जब एक बार बन जाती है, तो यह सामग्री मानो स्वयं अपनी कथा कहने लगती है और उसके पर्त खुलने लगते हैं। उपलब्ध स्थान की सीमा में अध्ययन का यह दृष्टिकोण भी यहां अपनाया गया है।
महाभारत ऐसा आकर ग्रन्थ है कि आद्यन्त उसके विषय का विवेचन करने के लिए बहुत अधिक स्थान, समय और शक्ति की आवश्यकता है। वैदिक साहित्य और चरण साहित्य के भी कई प्रकरण महाभारत में सुरक्षित बच गए हैं, जैसे आरण्यक पर्व का अग्निवंश अध्याय है, जिसकी व्याख्या स्कन्दजन्म की कथा के साथ कुछ विस्तार से यहां की गई। वस्तुतः महाभारत को पांचवां वेद ही कहा गया है।
जैसे समुद्र और हिमालय रत्नों की खान हैं, वैसा ही महाभारत भी है। जितना स्थावर और जंगम जगत् भारतीय दृष्टिकोण में आ सका था, वह महाभारत में इकट्ठा हो गया है। इसके निर्माता भगवान् द्वैपायन कृष्ण सत्यवादी और सर्वज्ञ थे, वे वैदिक यज्ञविधि और कर्मयोग के पारगामी थे, धर्म और ज्ञान के प्राचीन दर्शनों में सम्यक निष्णात थे। सांख्य और योग में उनकी पूरी गति थी, अनेक तन्त्र या शास्त्रों में उनका मन जागरूक था ।
ऐसे महाभाग बहस की यह कृति सचमुच महान् और सुविहित है। इसका जितना भी दोहन किया जाय, प्रतानुसार, उतने ही फल की उपलब्धि हो सकती है।
– वासुदेवशरण अग्रवाल
| Weight | 970 g |
|---|---|
| Author | |
| Language |


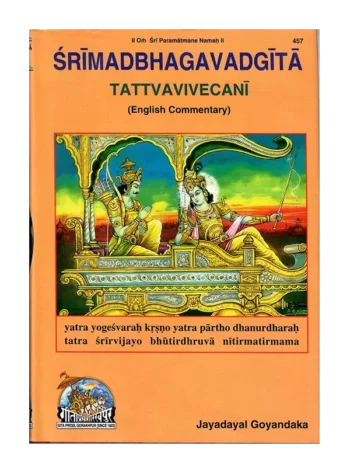
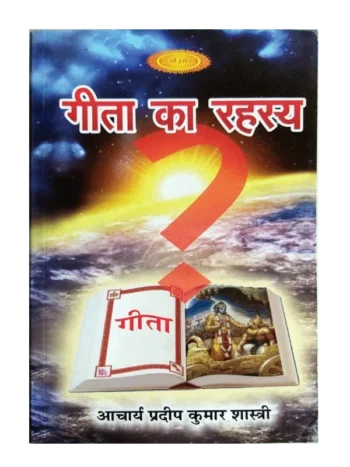
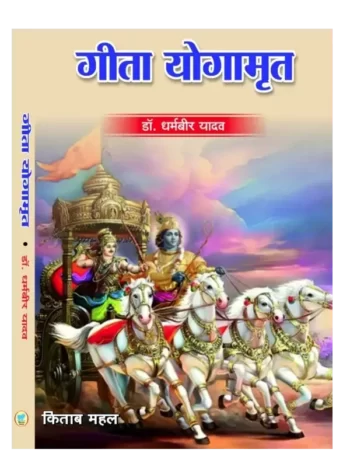
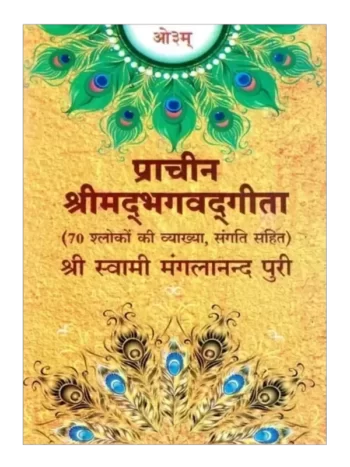

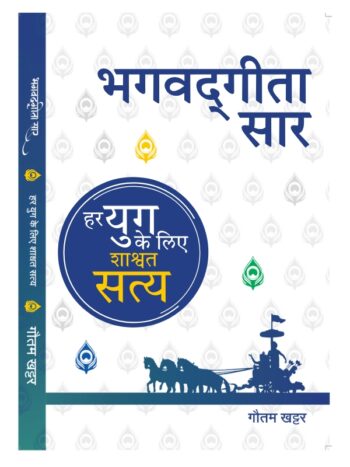
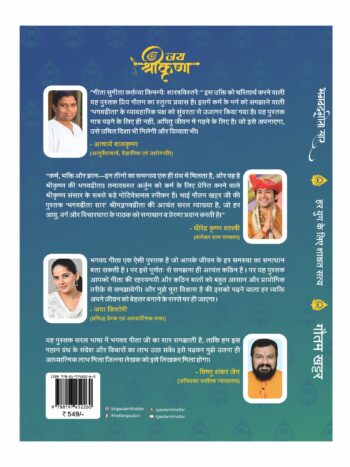
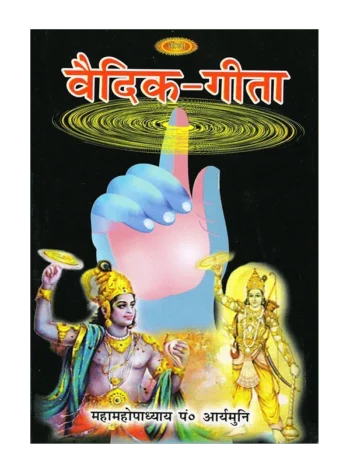
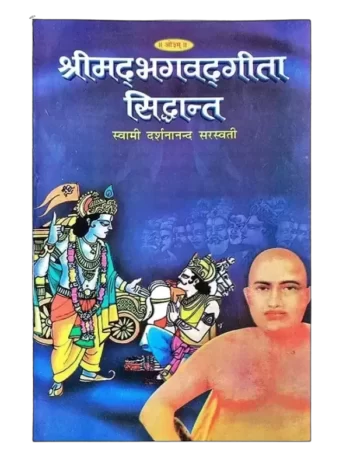
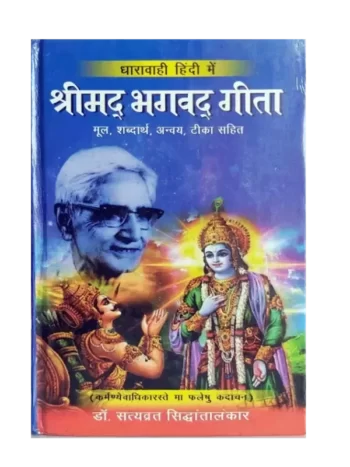
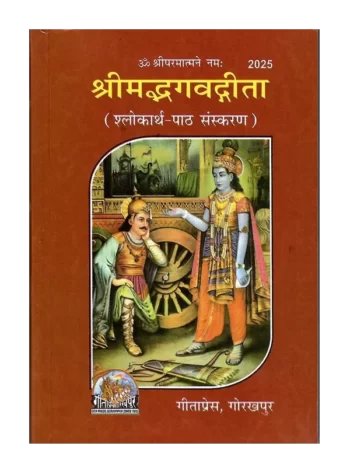
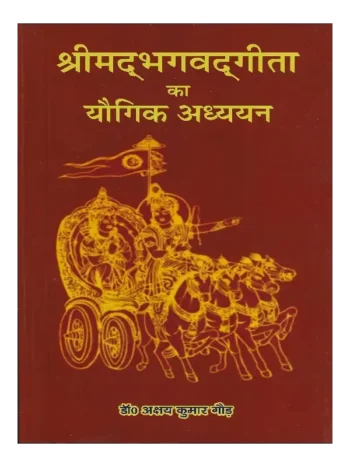
Reviews
There are no reviews yet.