भूमिका
‘योगवासिष्ठ’ भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म विद्या का एक ऐसा अनुपम ग्रन्थ है, जो अतिशय उच्च कोटि की महत्त्वपूर्ण रचना होने के बावजूद भी अत्यल्प प्रचलन में है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह प्रतीत होता है
कि यह ग्रन्थ अतिशय बृहद् है। प्राचीन छपी एक प्रति का भार तो लगभग सात-आठ कि.ग्रा. के बराबर होगा। ऐसे विशाल ग्रन्थ का पठन-पाठन एवं मनन-चिन्तन कर पाना कुछ ही लोगों के लिए सम्भव हो सकता है।
प्रमुखतः इसे अद्वैत वेदान्त का प्रतिपादक कहा जाता है। उस विषय के अन्य कई लघु ग्रन्थ बाजार में मिलते हैं, प्रायः उन्हीं से लोग इस सिद्धान्त का मत जान लेते हैं एवं ‘योगवासिष्ठ’ के अध्ययन जैसे समय एवं श्रम साध्य कार्यों से बचे रहते हैं।
एक अन्य बात यह भी है कि जन सामान्य की मान्यता है कि ‘योगवासिष्ठ’ वैराग्य की प्रेरणा देने वाला है। इसके अध्ययन से लोग अपना घर बार छोड़ने को सोचने लगते हैं। यद्यपि कुछ साधु वेषधारी ढोंगी लोग ग्राम एवं कसबों में योगवासिष्ठ के नाम पर ऐसी इधर-उधर की बातें सुनाते रहते हैं, जिससे लोगों की उक्त धारणा और भी अधिक पुष्ट हो जाती है।
ऐसी दो-चार घटनाएँ देख-सुन कर लोगों के चित्त में एक मिथ्या भ्रम पैदा हो जाता है तथा वे इसे गृहस्थाश्रम के लिए हानिकर मानने लगते हैं, जब कि यथार्थत: उसमें ऐसा कोई भी कारण नहीं है। निःसन्देह उसमें जगत् को सारशून्य एवं मायामय कहा है।
परन्तु इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे गृहस्थाश्रम या जागतिक व्यवहारार्थ अप्रिय कहा जा सके। यों तो लोग सत्य, अहिंसा, न्याय, क्षमा आदि को भी जागतिक लाभ की दृष्टि से हानिकर बताते हैं; लेकिन ऐसी वृत्ति उन्हीं की होती है, जिनकी दृष्टि सर्वदा स्वार्थ पर टिकी होती है तथा जिनका संसार दस-बीस गज लम्बे-चौड़े निज गृह तक ही रहता है।
अन्यथा जगत् में वही मनुष्य जीवित एवं जाग्रत् माने जा सकते हैं, जो अपने संग औरों के हित का भी पूर्ण ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग ही सभी के संग सहयोग एवं प्रेम का सम्बन्ध रखते हुए यथार्थ सुख पा सकते हैं।
निपट स्वार्थी लोग तो कभी उस सुख को नहीं पा सकते। अतः ‘योगवासिष्ठकार’ ने प्रतिक्षण यही उपदेश दिया कि जागतिक कर्मों को त्यागने की जरूरत नहीं है, उनमें आसक्त न होना ही ज्ञानी का स्वभाव है। इसी का वर्णन करते हुए ‘निर्वाण प्रकरण’ में कहा गया है।
‘वे ज्ञान सम्पन्न नहीं, मूढ़ हैं जो देह के स्थित रहने तक समुचित होकर देह की अवस्था के तहत कर्मेन्द्रियों को व्यवहत नहीं करते। जो अज्ञानी तत्त्व को नहीं पहचानते, वे स्वतः अज्ञानवश सहज अवस्थाओं से दूर भागते रहते हैं।
जब तक तिल हैं, तभी तक तेल है, उसी तरह जब तक देह है, तभी तक इसकी सहज दशाएँ भी रहेंगी। जो व्यक्ति देह की अवस्था’ के तहत व्यवहृत-कर्म नहीं करता, मानो वह खड्ग से आकाश को काटता है।
देश-दशानुसार मिलने वाले सुख-दुःख का त्यागना ही अनुचित है। चित्त की शान्ति एवं समत्व भावना तो योग द्वारा ही मिलती है न कि कर्मेन्द्रियों को प्रतिष्ठित कर देने से। जब तक देह है, तभी तक ज्ञानपूर्वक सदाचार के सहित कर्मेन्द्रियों द्वारा शरीर की जरूरतें पूर्ण करना चाहिए, मन से नहीं। जब तक सृष्टि है
तब तक कार्यों को करने से कोई भी दोष नहीं लगता। जब सभी कर्म प्रकृति के अधीन हैं, तो फिर उसमें दोष लगने की क्या बात है ?
इस प्रकार लेखक ने मात्र सहज कार्यों को निर्दोष ही नहीं कहा; वरन् पुरुषार्थ या कर्मवीरता को ही सभी तरह की उन्नति एवं सफलता का मूल बतलाया है।
‘इस जगत् में सर्व दुःखों का नाश करने के लिए पौरुष के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस जगत् रूपी धनागार में ऐसा कोई वेशकीमती पदार्थ नहीं हैं, जो परिष्कृत पुरुषार्थ से पाया न जा सके। हे महाबुद्धिमान् श्रीराम ! त्रिलोक में जो भी उत्तम पदार्थ हैं,
वे सभी दृढ़ भाव से किये गये पुरुषार्थ से पाये जा सकते हैं। जो जिस वस्तु के पाने की सच्चे मन से कामना करता है तथा उसे पाने हेतु सतत प्रयत्नरत रहता है, वह उसे निश्चित ही पा लेता है। इस संसार में शान्त बैठे रहने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता, जो जैसा यत्न एवं पुरुषार्थ करता है, वह वैसा ही फल पाता है, यथा-‘यो यो यथा प्रयतते स स तत्तत्फलैकभाक् ।’
‘कर्म’ की अनिवार्यता
जैसे पुष्प एवं उसके आशय में कोई भिन्नता नहीं है, वैसे ही कर्म एवं मन में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि एवं उसकी ऊष्मा पृथक् पृथक् नहीं है। कर्म ही पुरुष है तथा पुरुष ही कर्म है। इस तरह ये दोनों अभिन्न हैं, जैसे बर्फ एवं उसकी शीतलता। अतः यह जान लेना चाहिए कि दैव, कर्म, पौरुष आदि सभी एक ही तथ्य के पर्यायवाची हैं।
इस तरह ‘योगवासिष्ठकार’ ने सैकड़ों युक्तियाँ देकर यह कह दिया कि अद्वैत सिद्धान्त का यह अर्थ कदापि नहीं कि मानव, जगत् एवं उसके कर्मों को माया कहकर निकम्मा बन जाये एवं स्वतः पौरुष का त्याग कर समाज के लिए भार बन जाये।
परमेश्वर ने मनुष्य को कर्मेन्द्रियाँ एवं ज्ञानेन्द्रियाँ समुचित कर्म करने हेतु ही दी हैं। उन्हें निष्क्रिय रखना या उनसे कोई जनोपयोगी कर्म न करके अन्यों के श्रम के फल का उपभोग करना प्राकृतिक दृष्टि से एक असहज कृत्य ही नहीं; बल्कि समाज की दृष्टि से एक अपराध भी है।
कोई ज्ञानी व्यक्ति सामान्य लोगों को ऐसा विपरीत ज्ञानोपदेश नहीं दे सकता। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भिक्षा का पेशा करने वाले ‘साधु’ नामधारी लोगों ने ऐसी भी उक्तियाँ प्रचारित कर रखी हैं-
‘अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम। दास मलूका कह गये, सबके दाता राम ।।’ हमें नहीं मालूम कि यह उक्त तुकबन्दी मलूकदास की है अथवा किसी भिक्षाजीवी ने रचकर प्रचारित कर दी है। परन्तु इसमें जो भी ‘शिक्षा’ दी गयी है, वह बिलकुल ना समझी एवं व्यर्थ की है।
यदि यह मान भी लें कि अजगर एवं पक्षी कार्य नहीं करते, तो भी इसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि उनकी देखा-देखी मनुष्य भी कर्म न करें। अगर काम करने का आशय मात्र नौकरी व्यापार या मजदूरी करने से ही है, तब भी उक्त कहावत में कोई सार नहीं है।
कुछ सहस्र वर्ष पूर्व जगत् में आजकल जैसी नौकरी, व्यापार या मजदूरी का नाम भी नहीं था। सभी लोग जंगलों, पहाड़ों या फिर छोटी छोटी बस्तियों में स्वतन्त्र रूप से रहते थे तथा श्रम द्वारा जो कुछ जंगली फल-फूल, कन्द-मूल या शिकार प्राप्त कर सकते थे, उसी से अपना निर्वाह करते थे।
वनों में रहने वाले वन्य पशु- पक्षी भी अपने आहार को खोजने एवं पाने के लिए ऐसा ही अथक श्रम करते हैं। अतः यह कहना कि ‘साधु-सन्त’ बनने अथवा ‘आध्यात्मिक जीवन’ बिताने के लिए अकर्मण्य बने रहना ठीक है, ऐसा सोचना बिलकुल गलत एवं मूर्खता पूर्ण है। ऐसा केवल वे ही कह सकते हैं, जिन्होंने ‘हरामखोरी’ को अपना लिया है और ‘ठगविद्या’ या बेशरमी से अपना जीवन- यापन करना चाहते हैं।
कर्मों में आसक्ति का होना ही बन्धन ग्रस्तता है
मानव के लिए सतत कर्म करना सहज एवं अनिवार्य है; लेकिन वह जब उसमें आसक्त हो जाता है, हरेक कर्म से भाँति-भाँति की वासनाओं की पूर्ति की कामना करता है, तब वे (कर्म) दुःख एवं पतन के हेतु बन सकते हैं।
व्यक्ति की वासनाओं एवं इच्छाओं का कहीं भी अन्त नहीं है। एक के बाद दूसरी का पैदा होना स्वाभाविक है। उनकी पूर्ति असम्भव है। हम चाहे कितना भी श्रम एवं उद्योग क्यों न करें। परिस्थितिवश दश इच्छाएँ पूर्ण होंगी, तो दश अधूरी रह जायेंगी।
जो इच्छाएँ अपूर्ण रहेंगी, वे चित्त में असन्तोष पैदा करेंगी तथा उसके फल से एक के बाद एक विविध दुष्परिणाम सामने आयेंगे। इस प्रकरण को गीता में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है,
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽ भिजायते ।।
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशी बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।।
(गीता अ०२ / ६२-६३) अर्थात् ‘ भाँति-भाँति के विषयों की वासना रखने से उनमें आसक्ति का भाव प्रकट होता है और तभी उनकी पूर्ति की भावना भड़कती है। जब वह कामना पूर्ण नहीं होती, तब क्रोध जन्मता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का ह्रास एवं उससे बुद्धि का विनाश होता है। मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बुद्धि है। अतः जब बुद्धि विनष्ट हो जाती है, तब मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।’
‘योगवासिष्ठ’ में भी उक्त मत का समर्थन किया गया है। कर्म करने में स्वयं दोष नहीं; लेकिन उसमें आसक्त होना तो हानिकारक है। ‘निर्वाण प्रकरण’ में कहा गया है–
‘अज्ञानी को स्वयं के सभी कर्मों का फल इस कारण भोगना होता है; क्योंकि वह वासना के आधार पर कर्म पूर्ण करता है। परन्तु ज्ञानी की वासना क्षीण हो जाती है, तो उसे किसी भी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता।
वासना के अभाव में सभी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं, जैस जल के अभाव में लताएँ सूख जाती हैं। जैसे बेंत का लक्षण यह है कि उसमें फल नहीं आता, वैसे ही वासना शून्य कर्म निष्फल होता है। अनासक्त भाव रखने वाला ज्ञानी शुभाशुभ कर्मों को नित्य प्रति करता हुआ भी सांसारिक बन्धनों में नहीं फँसता, परन्तु जिस मूढ़ ने मन से इच्छाओं का परित्याग नहीं किया है
वह बिना कर्म किये ही सर्वदा जगत् रूपी सागर में डूबता रहता है। किसी विशेष फल प्राप्ति की कामना से जब व्यक्ति किसी कर्म को करता है, – तो जैसा उसका पुरुषार्थ होता है, तदनुसार ही वह फल प्राप्त करता है। कार्य का कर्त्ता होने से प्राणी उस फल का भोक्ता होता है। ”
– ‘गीता’ एवं ‘योगवासिष्ठ’ इन दोनों ने मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करने की सम्मति प्रदान की है, जिससे कर्म बन्धन में न पड़ना पड़े; परन्तु दोनों में अन्तर इतना जरूर है कि जहाँ गीता ने समस्त कर्मों का मूल स्रोत ईश्वर को मानकर कर्म करते रहने को सर्वोत्कृष्ट कहा है। वहीं ‘योगवासिष्ठ’ में ज्ञानी के लिए ‘कर्म’ ‘ अकर्म’ एक जैसे बताकर अन्तिम निर्णय व्यक्ति पर छोड़ दिया है–
” ज्ञानं नार्थ: कर्मत्यागैः नार्थः कर्मसमाश्रयैः ।
तेन स्थित यथा यद्यत्तत्तथैव करोत्यसौ ।
अर्थात् ज्ञानी व्यक्ति कर्म को छोड़ दे अथवा कर्म करने से कोई लाभ प्राप्त न हो, तो वह जब जैसा संयोग आ जाये, तब वैसा ही कर्म करता रहता है।’
सभी कर्मों का त्याग हो जाता है, सभी दुःख क्षीण हो जाते हैं। अतः मानव को ज्ञान द्वारा शुभाशुभ दोनों तरह के कर्मों का विनाश करना चाहिए।
यह तभी सम्भव होगा, जब पूर्व रूपेण हृदय में यह दृढ सङ्कल्प हो जाये कि कर्म कुछ भी नहीं है।
कहा भी गया है– गेहमेवोपशान्तस्य विजनं दूरकाननम् ।
अशान्तस्याऽप्यरण्यानी विजना सजना पुरी ।।
(निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध ३/३८)
अर्थात् ‘जिसका मन शान्त हो चुका है, उसके लिए घर में रहते हुए भी सुनसान कानन के सदृश अनुभव होता है तथा जिसका मन अशान्त है, वह जन शून्य वन में भी मानवों से परिपूर्ण नगरी की सी व्यस्तता की अनुभूति करता रहता है।’
गीता एवं योगवासिष्ठ का अनासक्तवाद
परन्तु ‘गीता’ में ज्ञानी के लिए कर्म अकर्म को एक जैसा मानने पर भी बाद में कर्म करने को श्रेष्ठ एवं आवश्यक कहा है–
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ।। नैव तस्य कृतेनार्थी नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असतो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।।
(गीता अ०३/१७ एवं अ०१८/१९ ) अर्थात् ” किन्तु जो मनुष्य स्वयं में रमण करने वाला एवं स्वयं में तृप्त और स्वयं में सन्तुष्ट है, उसके लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है। उस (महापुरुष) का इस जगत् में न तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है
और सभी जीवों में (किसी के भी संग) इसका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता। अतः तू सतत आसक्ति शून्य होकर कर्तव्य कर्म का सम्यक् रूपेण आचरण कर; क्योंकि आसक्ति शून्य होकर कर्म करता हुआ मानव परम तत्त्व को पा लेता है।”
‘कर्मयोग’ का यही दृष्टिकोण है। इसकी प्रतिद्वन्द्विता में दूसरे लोग ‘संन्यासपथ’ को ऊँचा बताकर पूर्व के दो श्लोकों का उदाहरण देकर यह पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञानी के लिये कर्म का त्याग करना श्रेयस्कर है।
‘योगवासिष्ठ’ में विविध स्थलों पर जगत् को मायारूप कहकर संन्यास मत का समर्थन किया गया है, तब भी उसका मूल आशय ‘कर्मयोग’ से मिला हुआ है। श्रीराम के कर्म त्याग की भावना का निस्तारण करते हुए श्री वसिष्ठ जी उन्हें बतलाते हैं-

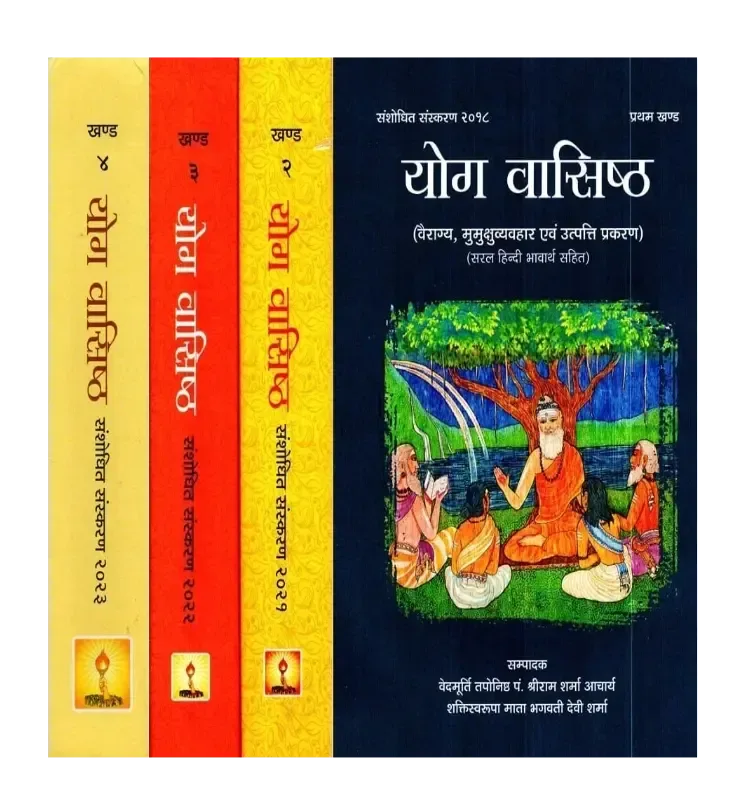

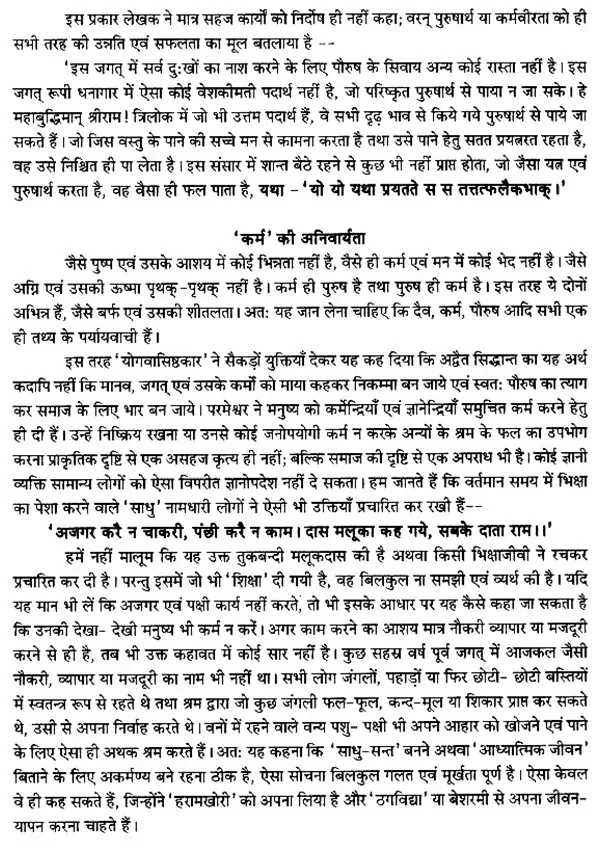
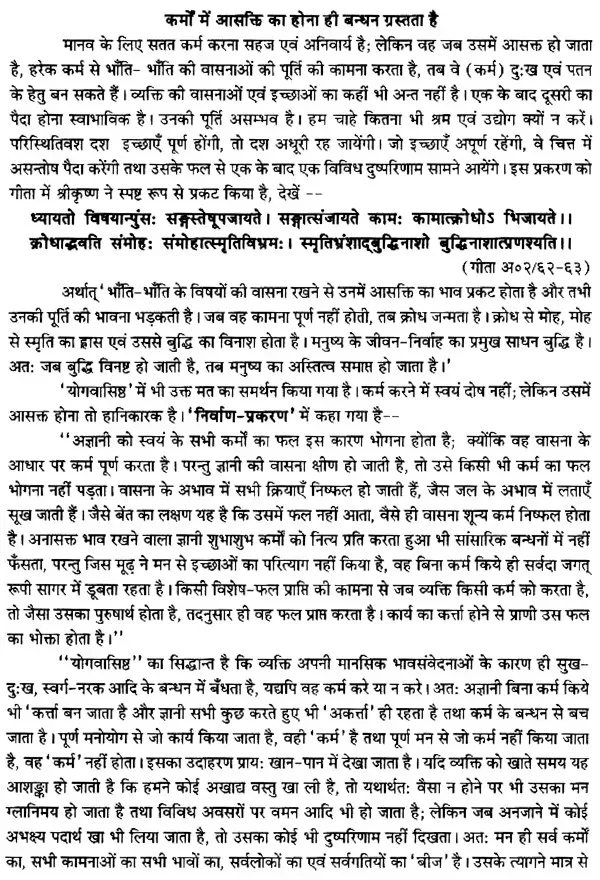
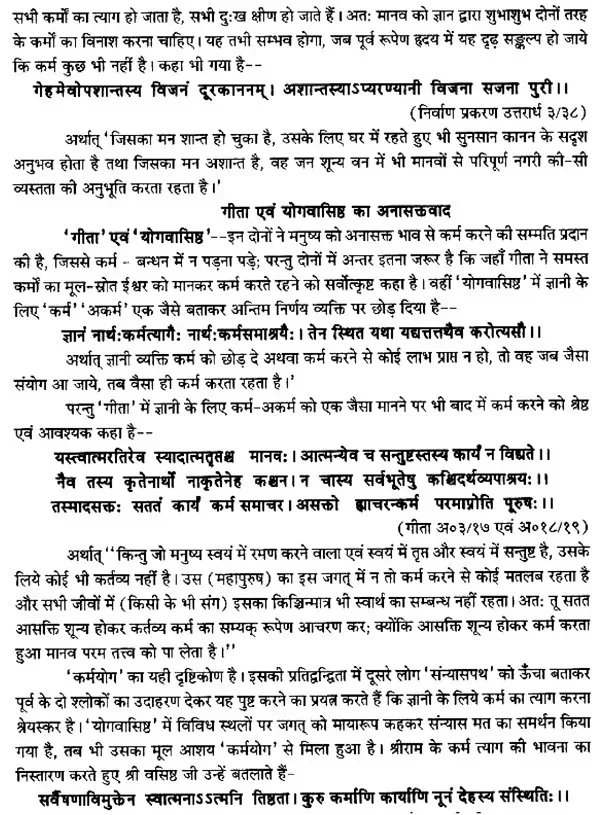

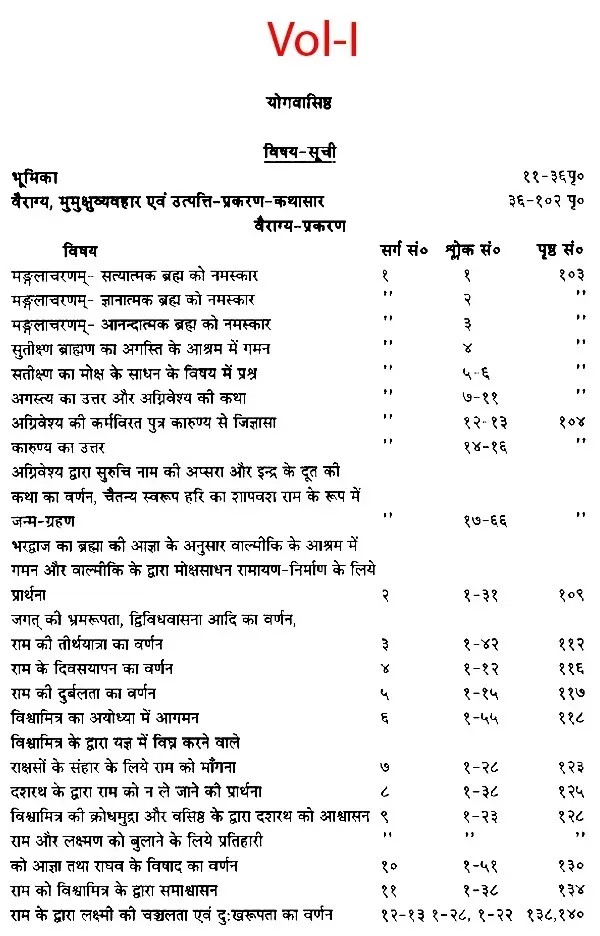
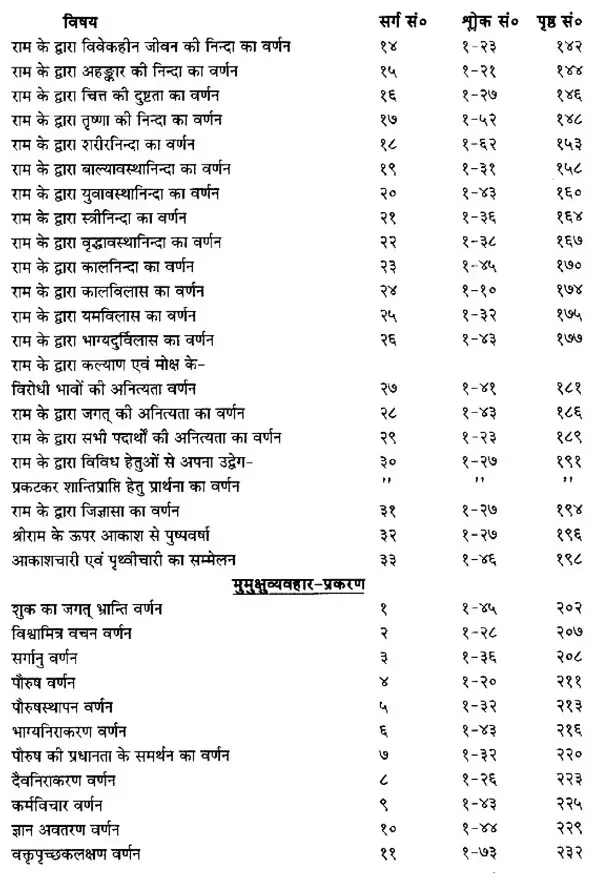
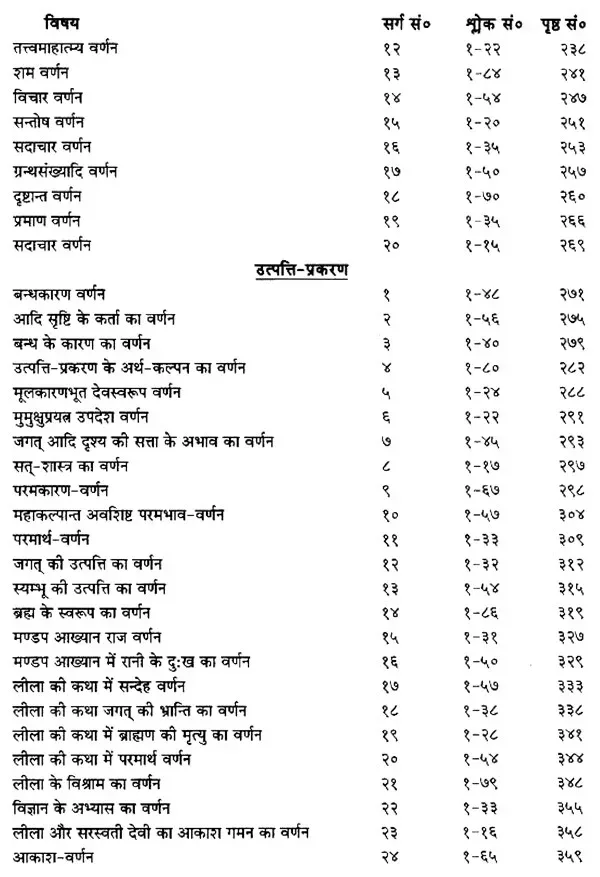
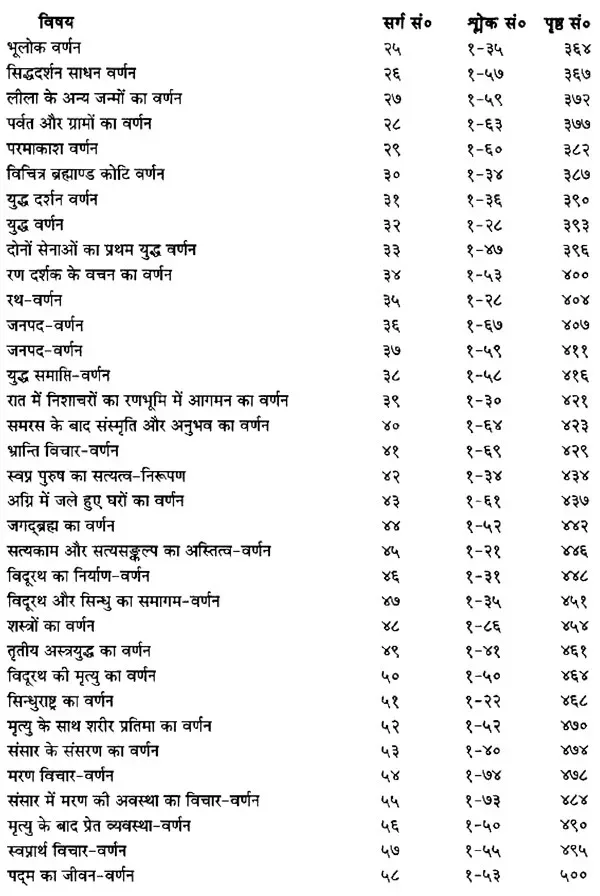
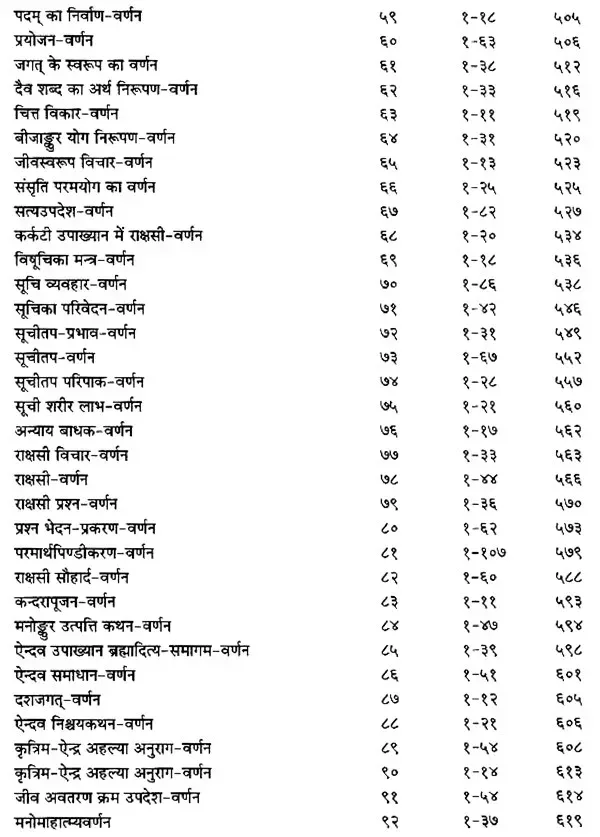
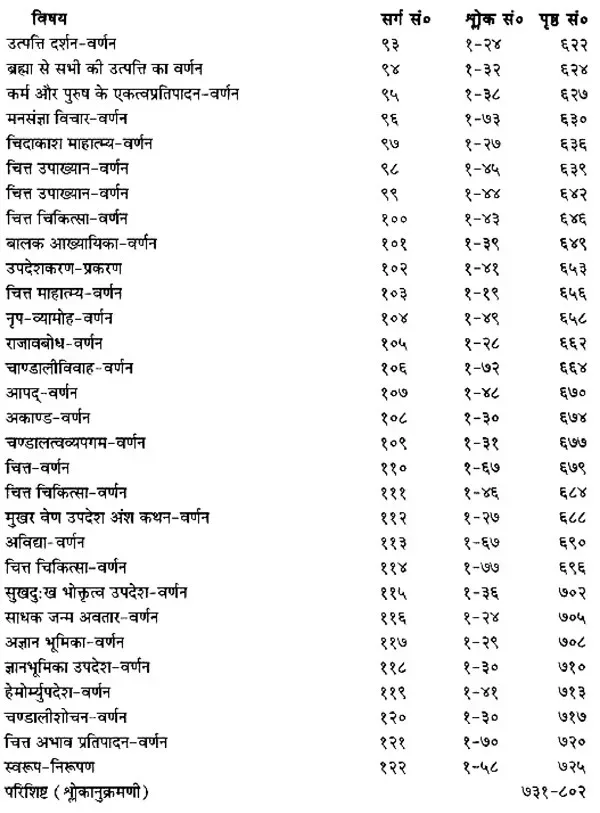

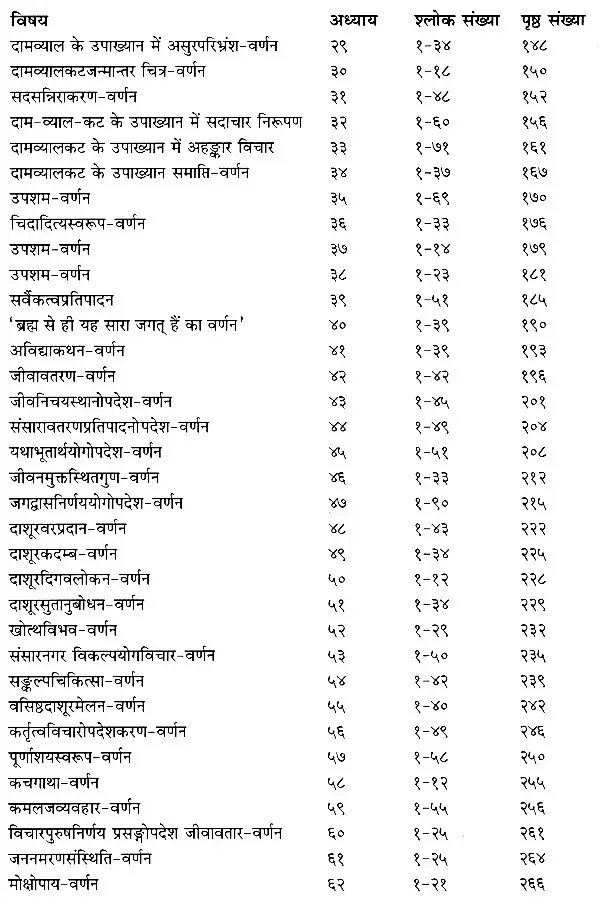

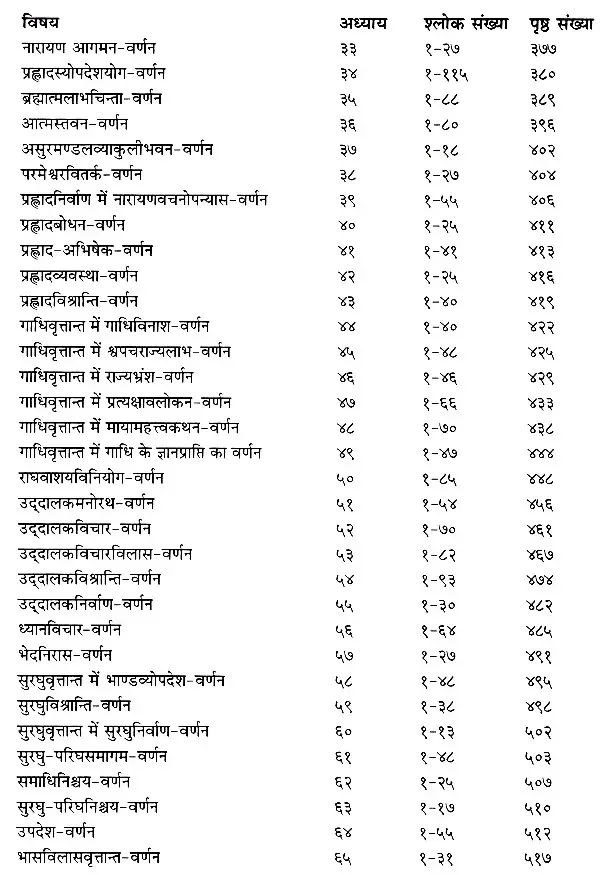
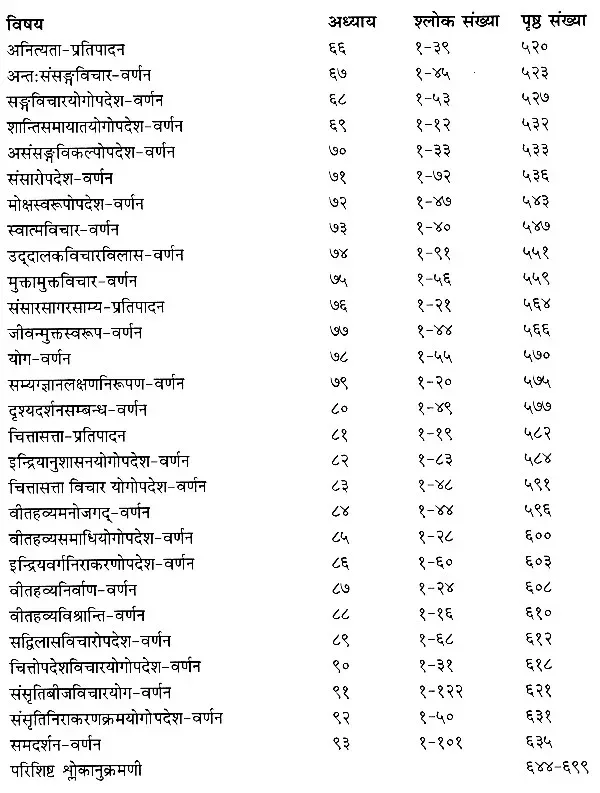

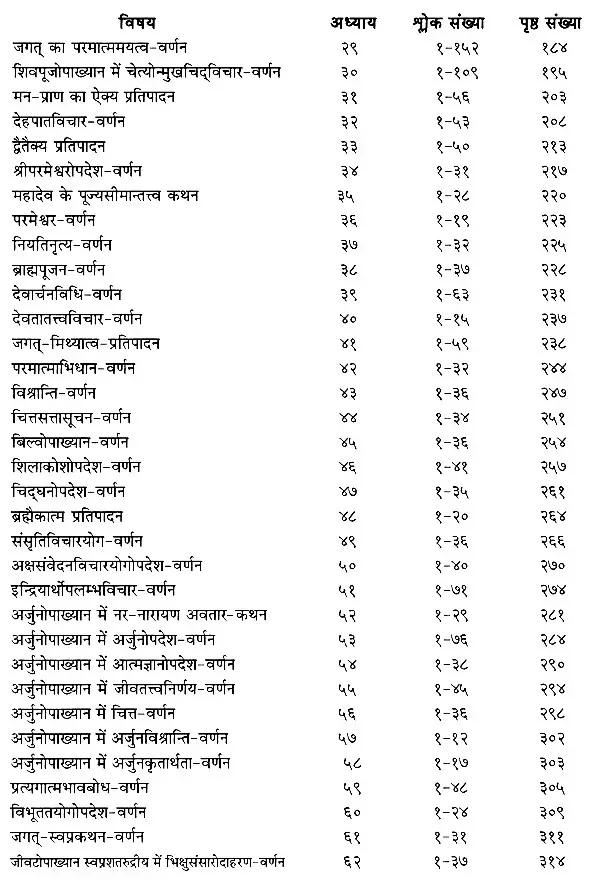
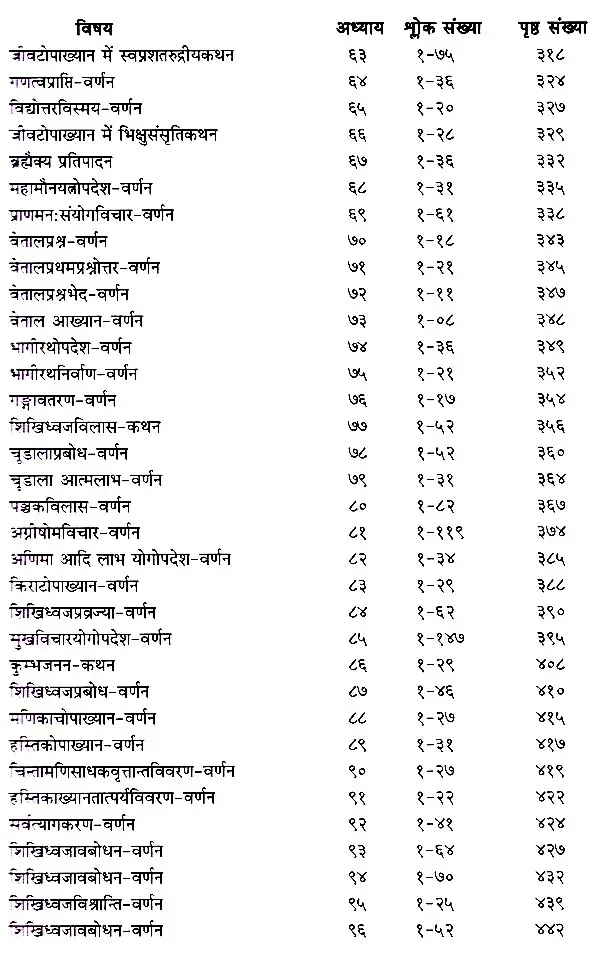
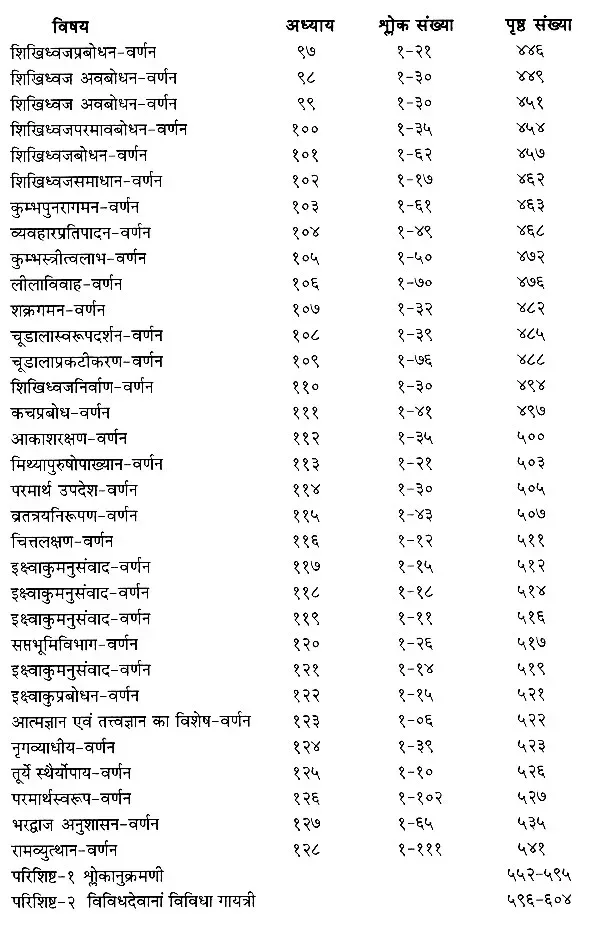

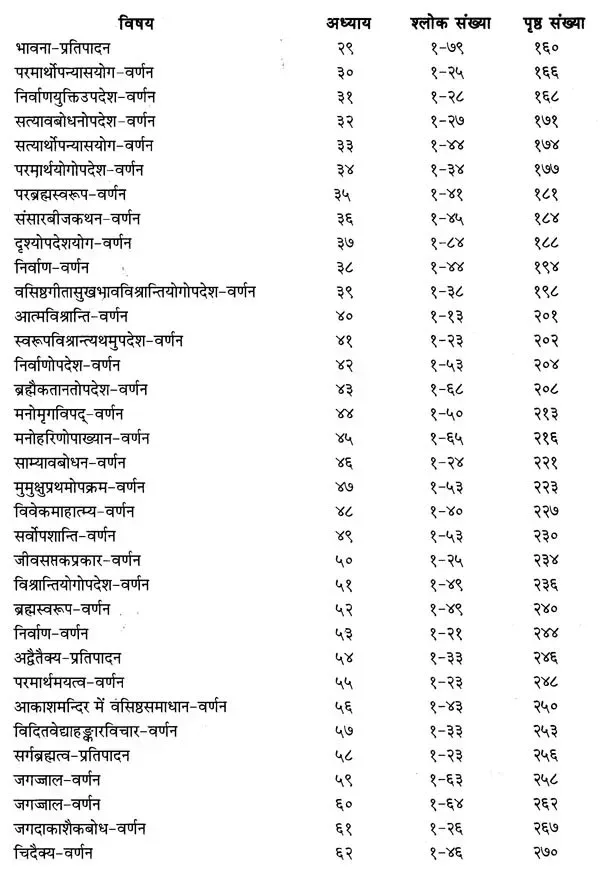
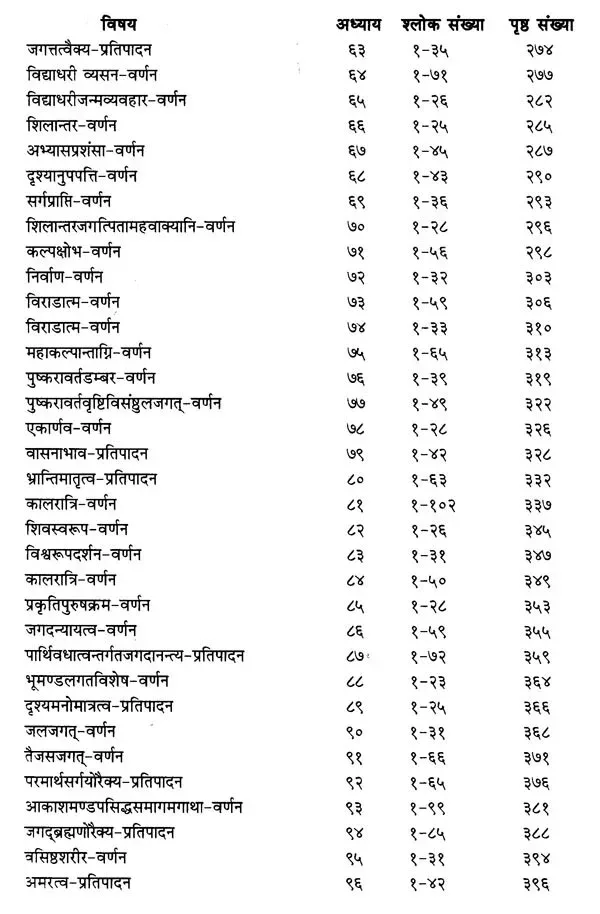
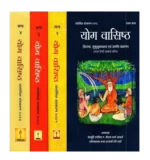























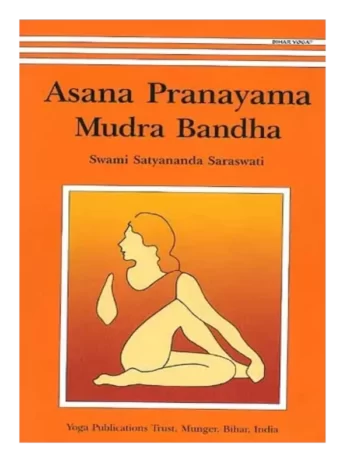
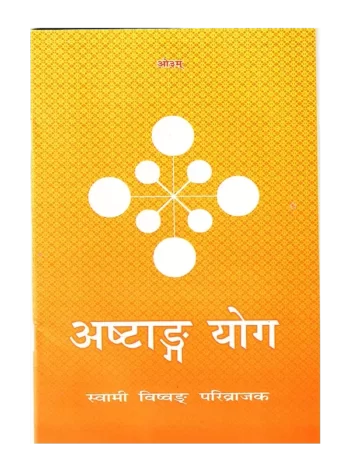
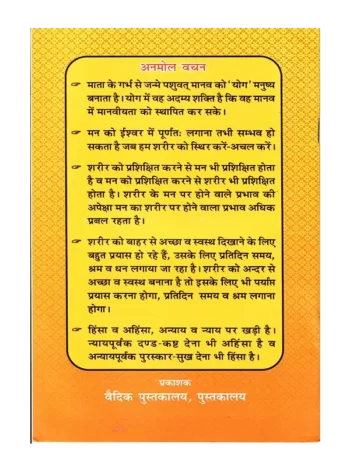
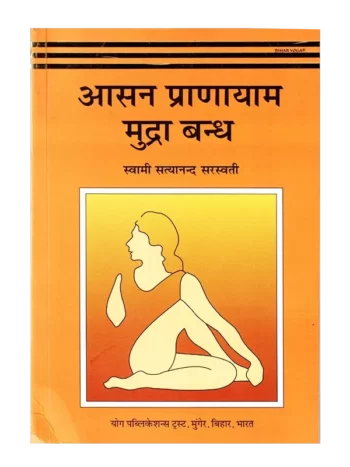
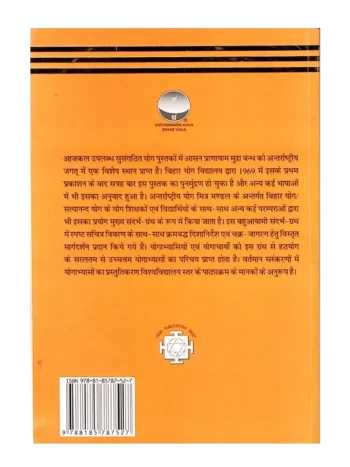

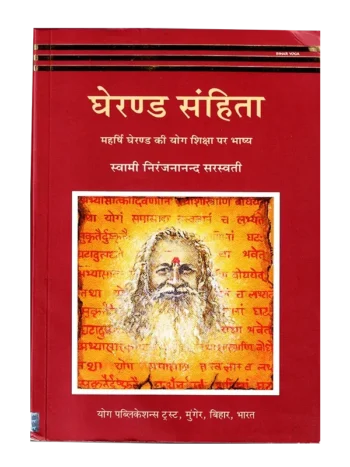
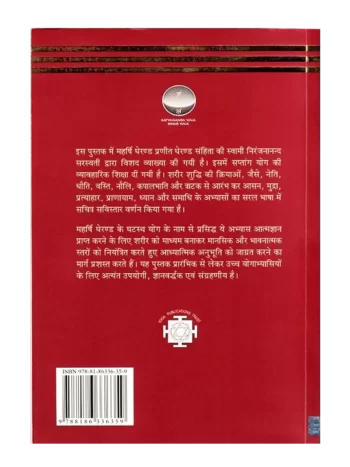
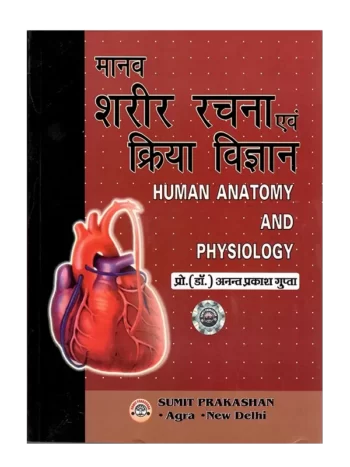
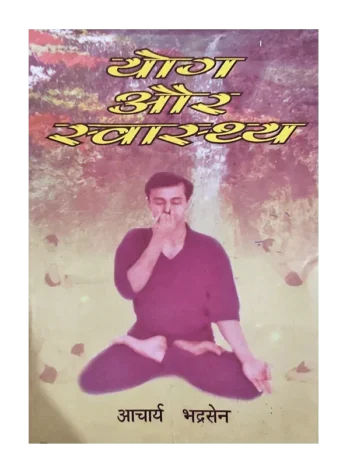
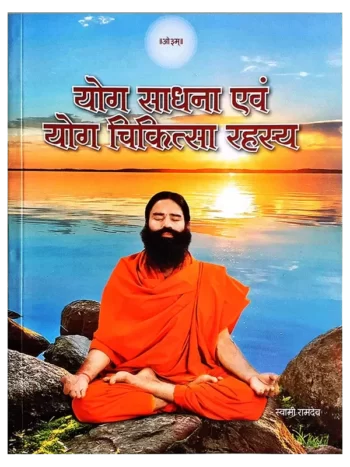

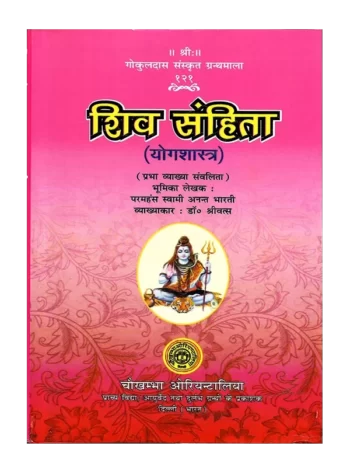
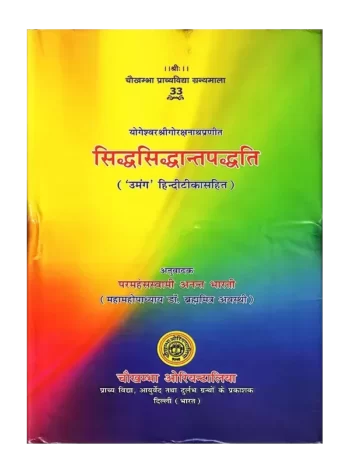
Reviews
There are no reviews yet.